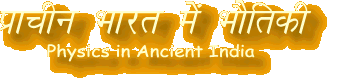
|
लेखक परिचय
डॉ० नारायण गोपाल डोंगरे डॉ० नारायण गोपाल डोंगरे का जन्म कर्नाटक प्रान्त के उडुपी जनपद स्थित 'नार्कट' नामक ग्राम में गुरुपूर्णिमा, संवत् १९९६ (१ जुलाई, १९३९) को हुआ। परन्तु ९ माह की अवस्था से ही वाराणसी में स्थायी रूप से निवास करते हुए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर (१९६०) तक की शिक्षा ग्रहण की। बाल्यकाल में वेदशास्त्रों के अध्ययन की पारिवारिक परंपरा के कारण उनमें संस्कृत भाषा के संस्कार रहे हैं। डॉ० डोंगरे श्री हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में लगभग ४० वर्ष से प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे तथा साह इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टिच्यूट के निदेशक के रूप में लगभग ३ वर्षों तक कार्य किया है। 'हिन्दू फिजिक्स' पर शोध कार्य के लिये सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) की उपाधि (१९७०) प्रदान की । साथ ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से भी भौतिकी में पी-एच.डी. की उपाधि (१९८५) प्राप्त की है। उनके अनेक सारगर्भित शोध-पत्र राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन भी किया है। डॉ० नारायण गोपाल डोंगरे ने भौतिकी के अध्ययन एवं अध्यापन के साथ-साथ पूरा जीवन प्राचीन भारतीय अभिलेखों के अध्ययन में व्यतीत किया है जो आगे भी जारी है। उन्होंने प्राचीन भारतीय अभिलेखों में स्थित विज्ञान ज्ञान को गणितीय सिद्धान्त व गणना के आधार आधुनिक विज्ञान के समकक्ष सिद्ध किया है। वैशेषिक दर्शन एवं अंशुबोधिनी पर इन्हें विशिष्टता प्राप्त है। 'वैशेषिक दर्शन का प्रशस्तपाद भाष्य' नामक प्राचीन परन्तु एक सामान्यतया उपलब्ध पुस्तक है जिसे अनेक जिज्ञासु अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन डॉ० डोंगरे ने वैज्ञानिक दृष्टि और चिन्तन से इसका अध्ययन कर और यह सिद्ध कर दिया है कि यह प्राचीन अभिलेख मात्र कुछ काल्पनिक ज्ञान का संग्रह भर ही नहीं बल्कि एक भौतिकी की पुस्तक है। इसी प्रकार उन्होंने महर्षि भरद्वाजकृत 'अंशुबोधिनी' ग्रन्थ (जिसकी मूलप्रति बड़ौदा राज्य के ओरिएंटल पुस्तकालय में उपलब्ध है) से एक वैज्ञानिक उपकरण को विकसित कर निर्मित किया है। डॉ० डोंगरे द्वारा मुख्य स्थापित उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं- वैशेषिक दर्शन से- १. लम्बाई, भार, समय तथा तापक्रम इकाई २. गति के नियम (जिसे न्यूटन) द्वारा प्रतिपादित गति के तीन नियम के रूप में जानते हैं) ३. इलास्टिसिटी का नियम ४. गुरुत्वाकर्षण का नियम (जिसे न्यूटन द्वारा प्रतिपादित रूप में ही जानते हैं) ५. रासायनिक क्रिया का सिद्धान्त (जिसे डाल्टन द्वारा परिभाषित एवं एवेगाड्रो द्वारा पुनर्परिभाषित के रूप में जानते हैं) ६. परमाणु का आकार (जैसा कि आजकल सुनिश्चित किया गया है) अगस्त संहिता से - वोल्टेइक सेल का विवरण, जल विघटन के द्वारा हाइड्रोजन व आक्सीजन उत्पादन कर हवाई यात्रा के लिए इससे गुब्बारा तैयार करना। अंशुबोधिनी से - १. ग्रन्थ में वर्णित वर्ण-क्रम-मापक (स्पेक्ट्रोमीटर) की संरचना के आधार पर रचना एवं निर्मिति जो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के मापन में सक्षम है। इस यन्त्र का अद्वितीय संयोजन विधान जो कि विभिन्न वर्ण के प्रकाश के लिए एक ही है जबकि आधुनिक पीढ़ी के स्पेक्ट्रोमीटर के लिए विभिन्न वर्णों हेतु अलग-अलग संयोजन अपेक्षित होता है। २. एक आर्द्रता-प्रभाव-मुक्त अवरक्तक्षेत्र में पारदर्शी काँच ग्रन्थ में निर्दिष्ट संरचना विधान से बनाया गया है जो अभी तक अज्ञात था। ३. ग्रन्थ में सौर-वर्णक्रम (Solar Spectrum) में उपस्थित कृष्ण रेखाओं का संप्रति ज्ञात फ्राउनहॉफर-रेखाओं की अपेक्षा विस्तृत विवरण एवं निबन्धन। ४. अणुओं के केन्द्रकों (Nuclei) की संरचना का विस्तृत विवरण (जिस पर आंशिक अध्ययन हो गया है व अभी शोध कार्य जारी है)। उल्लेखनीय है कि डॉ० डोंगरे की उपर्युक्त उपलब्धियाँ एवं गणनाएँ सन्दर्भ ग्रन्थ के अनुवाद मात्र से प्राप्त नहीं हुई हैं बल्कि यह एक वैज्ञानिक विशिष्टता, चिंतन तथा दृष्टि का परिणाम है। इनका यह प्रयास 'एकला चालो रे' के सिद्धान्त पर आधारित है। उनका मानना है कि हमारे प्राचीन अभिलेखों में स्थित ज्ञान के खजाने को बाहर लाने के लिए एक ऐसे छात्र समुदाय द्वारा सतत अध्ययन की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक ज्ञान रखने के साथ-साथ वैज्ञानिक चिन्तन, दृष्टि तथा संस्कृत व्याकरण का उत्कृष्ट ज्ञान भी रखते हों। उनका कहना है कि हमारे प्राचीन खजाने में मात्र प्रस्तुत ज्ञान भर ही नहीं है, वह तो असीम है। इस प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी लाभान्वित हो सके अन्यथा यह ज्ञान भण्डार सदैव के लिए समाप्त हो जायेगा और मात्र कुछ लोग इसे पूजा-अर्चना के रूप में पढ़ते रह जायेंगे। |